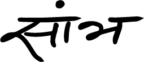● टांकरी लिपि का परिचय ●
टांकरी लिपि उत्तर भारत में अर्वाचीन काल मे प्रचलित होने वाली लिपि रही है। लिपि और भाषा पर अनेकों बार लोग भ्रमित होते देखे गए हैं। वरन इस अंतर को अन्यान्य विद्वानों द्वारा बारंबार स्पष्ट करने के उपरांत भी टांकरी को भाषा कहने की त्रुटि लोग सहज ही कर जाते हैं। यह लिपि पहाड़ों में मुख्यतः 15वीं से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अधिक प्रयोग की गई है। इसके उद्भव और प्रचलन में आने वाले कालखण्ड के विषय मे शोधकर्ताओं द्वारा शोध करके अनुमान लगाया गया कि यह लिपि 14वीं ईस्वी के आसपास प्रचलन में आई और 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में प्रचलित रही। इसका प्रयोग पारंपरिक रूप से डोगरी, चंब्याली, मंडयाली, जौनसारी, कुलुवी इत्यादि पहाड़ी बोलियों को लिपिबद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा।
टांकरी लिपि शारदा परिवार की लिपि मानी जाती है, जिसका सम्बंध गुरुमुखी और उसकी पूर्वलिपि लांडा से है। शारदा एवं टांकरी लिपि नामक अपनी पुस्तक में लिपिविद एवं शोधकर्ता कौल डेआम्बी टांकरी के विषय मे अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं “टांकरी का उद्भव 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ है।” वहीं प्रसिद्ध पुरातत्विक शोधकर्ता वोगल ने भी इसे 13वीं शताब्दी के आसपास का ही माना है। इस लिपि की उत्पत्ति के संदर्भ में ब्युहलर और ओझा का मत है कि यह शारदा लिपि की वंशज है। यह सत्य है, इसलिए सभी ने इसे शारदा लिपि का घसीट रूप माना है। दोनों लिपियों के अक्षरों की बनावट में तुलना करके इसकी आसानी से पुष्टि की जा सकती है।
13वीं 14वीं शताब्दी के आरम्भ में जिस समय इस लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है उस समय इस लिपि के स्वरूप को टांकरी ना कहकर ‘देवशेष’ कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि आरम्भ में देवशेष लिपि का प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों और राजकीय कार्यों के लिए किया जाता था। जबकि बाद में प्रचलित हुई टांकरी का प्रयोग इसके अलावा व्यापारिक और अनौपचारिक कार्यों को लिपिबद्ध करने के लिए किया जाता था।
देवशेष नाम का वर्णन लगभग सभी शोधकर्ताओं और विद्वानों ने अपने आलेख में किया है। परंतु देवशेष कहा क्यों जाता था इसपर किसी ने भी प्रकाश डालने का प्रयत्न नहीं किया। यहां प्रश्न यह है, यदि यह लिपि शारदा का स्वरूप थी तो इसे उससे संबंधित मिलता जुलता नाम क्यों नहीं मिला ? इसका कारण; सम्भवतः नाम व्युत्पत्ति में तथ्यों तर्कों का अभाव रहा होगा, इसलिए देवशेष नाम पर अधिक चर्चा ना हो सकी।
देवशेष के सम्बंध में हम यह देखते हैं कि शारदा लिपि को जम्मू-कश्मीर के मौखिक प्रचलन में देव-लिपि भी कहा जाता था। इसके अक्षरों की बनावट को ध्यान से देखें तो कश्मीर के शैव दर्शन के 36 तत्वों की छाप इन अक्षरों पर दिखती है। इस छाप को देखने के लिए ब्राह्मी लिपि और शारदा के अक्षरों का सापेक्ष अध्ययन दर्शन शास्त्र के अनुसार करने पर यह सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है। एक पक्ष के अनुसार यहां हम केवल इतना देखें कि देव लिपि के मूल स्वरूप से जो लिपि शेष रही वह देवशेष कहलाई। निःसंदेह इस विषय पर मतांतर हो सकते हैं। परंतु यह मतांतर भी वैसे ही हैं जैसे टांकरी के मूल उत्पत्ति पर हैं। सबने अपने-अपने पक्ष दिए हैं अतः यह भी एक पक्ष है, अपने शास्त्र और दर्शन अनुसार लिपि को केवल लिपि ना मानकर उसे मातृका रूप में सम्मान देने का। जिस रूप में कश्मीर शैव मत का दर्शन मातृका की व्याख्या करता है उसमें शारदा के अक्षरों की बनावट इसी से सम्बद्ध दिखती है।
टांकरी लिपि को मूलतः टाकरी कहने का रिवाज़ है। इसके पीछे का कारण है, इसका उद्भव क्षेत्र। परंतु यहां भी शोधकर्ताओं द्वारा अधिकतर दो व्युत्पत्तियों का सुझाव दिया जाता है। टांकरी लिपि के विषय मे एक मत है कि यह वर्तमान पाकिस्तान के टका प्रदेश से उत्पन्न हुई लिपि है। दूसरा मत इसका सम्बन्ध टंका अर्थात एक वाणिज्यिक शब्द के रूप में इंगित करता है। यह शब्द महाजनी शब्द के समानान्तर भी प्रस्तुत किया गया है। एक मत यह भी प्रचलन में आया है कि महाजनों के टंकण की लिपि होने के कारण इसे यह नाम मिला है। एक अन्य मत इसे संस्कृत के ‘ठक्कुर’ शब्द से जोड़ता है। राजपूत जमीदारों के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था। अतः इस लिपि को ठाकुरों की लिपि भी कहा गया।
अंशुमान पांडे ने इस लिपि के उद्भव के लिए uncertain etymology शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात इस लिपि के उद्भव पर निश्चित एवं निर्णयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। वोगल का संदर्भ देकर वे कहते हैं कि वोगल ने इसे टंका (सिक्का या वाणिज्यिक रूपक) से जोड़ा है और ग्रियर्सन ने इसे टक्का (प्रदेश या जाति) से जोड़ा है।
टांकरी लिपि के उत्पत्ति के संदर्भ में अभी तक यही निष्कर्ष निकलता है कि इसकी उत्पत्ति के कारक और कारण संशयात्मक आलोक में विचार रहे हैं। जिसे सम्भवतः किसी शोधकर्ता द्वारा भविष्य में प्रमाणिक शोध द्वारा जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके उद्भव के विषय मे कोई उसके बाद ही निर्णयात्मक वाक्य रखने के लिए अधिकृत होगा। अतः यह स्पष्ट है कि इस लिपि के उद्भव और नाम व्युत्पत्ति को लेकर अभी कोई स्पष्ट एकमत नही है। सम्बंधित सभी आकलन संभावनाओं के आधार पर हैं। इतना अवश्य है कि यह लिपि शारदा लिपि का एक घसीट स्वरूप है या कहिए शारदा के तात्कालिक स्वरूप की आशुलिपि समान है।
● हिमाचल प्रदेश में टांकरी लिपि ●
हिमाचल प्रदेश में टांकरी लिपि का इतिहास कब आरम्भ हुआ उसके लिए हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, वे हैं; यहां मौजूद अभिलेखों की श्रृंखला और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में विभिन्न लोगों द्वारा सहेजी गई पांडुलिपियां। इसके साथ ही पहाड़ी मंदिरों में टांकरी अभिलेखों और देवी-देवताओं (mask inscription) के अध्ययन करने से भी इस लिपि का हिमाचल में इतिहास जाना जा सकता है। राजाओं द्वारा की गई परस्पर संधियों में कब और कहां किस लिपि का प्रयोग हुआ है, इसका भी लिपि विकासक्रम को समझने में उपयोग होता है।
हिमाचल में टांकरी लिपि के अलावा वैसे तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, कुटिल, शारदा, नागरी, पाबूची, भट्टाक्षरी, पण्डवानी, चंडवानी, भोट इत्यादि लिपियाँ विद्यामान रही हैं। जिनके साक्ष्य यहां के अभिलेखों और पांडुलिपियों में निबद्ध हैं। परंतु मूल रूप से सामान्य व्यवहारिक प्रचलन में जो लिपियाँ मध्यकाल से यहां प्रचलित रही हैं उनमें टांकरी, भोटी, पण्डवानी, चण्डवाणी, भट्टाक्षरी और पाबूची प्रमुख रही हैं। ये सभी लिपियाँ या तो शारदा लिपि से उद्भूत हुई हैं या उससे संबंधित हैं। वर्तमान शोधात्मक प्रसंगों में टांकरी और पाबूची इन दो हिमाचली लिपियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इनमें भी अधिक ध्यान टांकरी पे दिया जा रहा है क्योंकि टांकरी अपने विभिन्न स्वरूपों में, पाबूची के विपरीत पूरे पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित लिपि रही है। पाबूची जहां अपनी साञ्चा विद्या के कारण सिरमौर और शिमला के चौपाल क्षेत्र में अधिक जानी जाती है, वहीं टांकरी एक समय सामान्य जन की लिपि के रूप में अधिक प्रचलित होने के कारण प्रसिद्ध हुई। एक मत यह भी है कि पाबूची सिद्धमातृका से उद्भूत है और टांकरी शारदा लिपि से।
लिपिबद्ध श्रृंखलाओं को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि हिमाचल प्रदेश का वर्तमान चंबा ज़िला लेखन एवं कला का प्रमुख केंद्र रहा है। अतः इस आधार पर अनुमान लगाकर इसे हिमाचल में टांकरी का प्रवेशद्वार कहा जा सकता है। हिमाचल में टांकरी पर वर्तमान में सर्वाधिक तथ्यात्मक कार्य करने वाले डॉक्टर किशोरी चंदेल के लिखित आलेखों में इस लिपि के हिमाचल में आने से लेकर इसके प्रयोग तक सबकुछ क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अपने शोध द्वारा हिमाचल में टांकरी का उद्भव मध्यकाल माना है।
यदि हम तर्कसम्मत दृष्टिकोण से देखें तो हमें टांकरी के पूर्ववर्णित उद्भवकाल और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अभिलेखों और पांडुलिपियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि टांकरी के आरंभिक स्वरूप देवशेष का प्रचलन जम्मू और चंबा के इलाके में रहा है। वहीं से इसका विस्तार हुआ। जम्मू में इसे डोगरी लिपि के रूप में ख्याति मिली। डोगरी का मानकीकरण होने के साथ वह पिछले 2-250 वर्षों में सशक्त रूप से स्थापित होने में कामयाब रही। जबकि टांकरी को इस प्रकार का सौभाग्य नहीं मिल पाया। मध्यकाल में जब गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद देव द्वारा मानकीकृत किया गया, उस समय टांकरी पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रानुसार परिवर्तन कर नए नए रूप में स्थापित हो रही थी।
● टांकरी लिपि के प्रकार ●
शारदा के तत्काल परिवर्तित स्वरूप देवशेष को देखें तो हम पाएंगे कि टांकरी लिपि भी मूलतः एक ही प्रकार की थी। जिसके अक्षरों में परिवर्तन समय के साथ आया। यहां शोधार्थियों और मेरे निजी मत में अंतर है। सिद्धान्तवादी और शोधार्थी इस विषय मे उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर टांकरी के प्रकारों का उल्लेख करते हैं। इस सम्बंध में कोई भी अपवाद नहीं। सभी एकमत से टांकरी के विकासक्रम को लेकर क्षेत्रीय परिवर्तन पर पक्ष निर्धारित करते हैं। लिपि में प्रकारों को लेकर एक अवधारणा यह भी है कि सबने लिखने के लिए अपने तरीके ईजाद अवश्य किये होंगे; अतः लिपि के विभिन्न रूप प्रचलित हुए। परंतु यहां हमें लिपि के प्रकारों से अधिक उसके विकासक्रम के सामाजिक, व्यवहारिक एवं अन्यान्य पहलुओं का सापेक्ष मूल्यांकन करना होगा। पहले लिपि का प्रयोग अधिकतर शिलालेख, काष्ठफलकों पर लिखने के लिए या विभिन्न धातुओं पर इसे उकेरने के लिये किया जाता था। यह ध्यान देना आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति इसे लिखता था, वह इसके बारे में कितना जानता था या उसकी कला में लेखन का प्रयोग कितना होता था? पत्थर पर उकेरी जाने वाली आकृतियों के लिए कौन सा औज़ार प्रयुक्त होता था? सम्बंधित कलाकार की दक्षता क्या थी ? काष्ठकला में सिद्धहस्त कारीगर लिपि को कितना जानते समझते थे और लिपि लेखन में कितने निपुण थे ?
वस्तुतः यहां व्यवहारिक ज्ञान और सहज ज्ञान का प्रश्न अधिक है। मेरा मानना है कि लिपि परिवर्तन का मुख्य कारण एक ही है और वह है; लिखावट की त्रुटि। लिखावट की त्रुटियों का लिपि परिवर्तन में 90 प्रतिशत योगदान है। कालांतर में किसी भी लिपि में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तन आया हो तो उसके परिवर्तन के विकासक्रम पर हम दृष्टि डालते हैं।
यथा : टांकरी लिपि में ‘ज’ अक्षर की बनावट शारदा लिपि के ‘ज’ के बाईं ओर झुकने से हुई है। टांकरी का ‘ज’ रोमन लिपि के ‘E’ के समान है, जो दाईं ओर को कुछ झुकाव लिए हुए है। परंतु यह झुकाव आने में भी कम से कम 100 वर्षों का समय लगा ही होगा। यही ‘ज’ वर्तमान में टांकरी के चंब्याली प्रकार में ‘ऊ’ समान दृष्टिगोचर होता है। जिसका कारण ‘E’ की खड़ी रेखा को किसी अभिलेख में कारीगर द्वारा कुछ मोड़ देने के कारण बाद के पढ़ने वाले को ‘ऊ’ प्रतीत हुआ होगा। अतः परिवर्तन का कारण अनुमान, भ्रम और लेखन में त्रुटि प्रतीत होता है। इसी प्रकार यदि हम टांकरी लिपि की मात्राओं को देखें तो यहां भी परिवर्तन का कारण
मानकीकरण द्वारा इसे परिवर्तित करना नहीं अपितु मात्राओं के लेखन में आई त्रुटियां हैं। टांकरी की बाराखड़ी में ‘ओ’ की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर एक पक्षीनुमा चिन्ह बनाकर लगाई जाती है। यहां इसमे और शारदा लिपि में ‘ओ’ की मात्रा में अंतर केवल इतना है कि जहां टांकरी में यह मात्रा अक्षर की शिरोरेखा से ऊपर रहती है वहीं शारदा में यह मात्रा शिरोरेखा के दाएं भाग को थोड़ा काटकर नीचे की ओर प्रवेश करती है। अभिलेख लिखते समय किसी से यह कटान ना हुआ होगा और इसी का अनुसरण करते हुए पीछे मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाने लगी।
एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर गौर करना आवश्यक है। हमें यह भी देखना होगा कि जिस समय टांकरी लिपि पहाड़ों में विस्तार ले रही थी, उस समय इसे लिखने वाले और पढ़ने वालों की संख्या क्या रही होगी या लेखन कर्म कितने लोगों के ज़िम्मे था। टांकरी की कुछ पांडुलिपियों को पढ़ें तो उनमें लिखने वाले के लेखन में उर्दू अक्षर लेखन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।
यथा : चंबा भूरी सिंह संग्रहालय में मौजूद पांडुलिपि ‘तवारीख़ मुलख़ कुल्लू’ के लेखक वज़ीर जीतू दियारी और सहायक कायथ भंगालिया टांकरी के अक्षरों के अंतिम छोर को उर्दू-फ़ारसी के अक्षरों समान अंत मे घसीटकर लंबा ले जाते हैं।
इसी प्रकार उदाहरण के रूप में डॉक्टर किशोरी चंदेल जी के शोध प्रपत्र ‘The mask inscriptions of The Western Himalaya : A case study of some inscribed mohra’s of Kullu’ में देवी देवताओं के मोहरों पर अंकित टांकरी के प्रारूपों को तालिकाबद्ध किया गया है। प्रपत्र में दिखाए गए मोहरों का अध्ययन करने पर हमें स्पष्ट होता है कि एक ही कालखण्ड में कुल्लू के भीतर मोहरों पर लिखे गए अक्षरों की बनावट तक मे अंतर है।
उदाहरण स्वरूप, 1762-63 में कुल्लू के राजा टेढ़ी सिंह द्वारा देवता त्रिजुगी नारायण (दियारी ठाकर,दियार) और आदि ब्रह्मा (खोखण) देवताओं को भेंट स्वरूप एक-एक मोहरा दिया गया था। देवता दियारी ठाकर जी के मोहरे पर जहां राजा टेढ़ी सिंह का नाम अंकित है वहां नाम के मध्य ‘ज’ अक्षर के लिखने के तरीके में थोड़ा अन्तर है। उसी प्रकार ‘टेढ़ी’ के ‘ट’ की बनावट एक जगह छोटी और तीक्ष्ण स्वरूप में है और दूसरी जगह चौड़े स्वरूप में। अतः यह स्पष्ट है कि दोनों अंतर कारीगर की लेखन त्रुटि और परिस्थितिजन्य हैं। इसमे लिपि के लिप्यान्तरण का कोई किरदार नही माना जा सकता। अन्य समकालीन मोहरों और अभिलेखों का मूल्यांकन करने पर यह अंतर साफ़ दिखाई देता है। ग्रियर्सन के दृष्टिकोण से हमें पता चलता है कि यह लिपि क्षेत्रीय परिवर्तनों के बावजूद सभी जगह अपनी एक अंतर्निहित संरचना के अंतर्गत प्रचलित है। अतः हम इसे लिपि के प्रकार ना कहकर एक वर्ग विशेष के अंतर्गत मान सकते हैं।
लिपि के विकासक्रम और परिवर्तन के बारे में हमें A. K. Singh की पुस्तक ‘Development of Nagari Script’ से व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। जहां उन्होंने नागरी लिपि के ब्राह्मी लिपि से अभी तक के परिवर्तनों को तालिकाओं में चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है।
लिपि के विभिन्न अंतर अवलोकन के इस दृष्टिकोण के अलावा लौकिक परिस्थितियों से हमें मूलतः इसके कुछ एक प्रचलित प्रकार प्राप्त होते हैं। जिसमे चंब्याली, कांगड़ी, जौनसारी-सिरमौरी, कोची, मंडयाली, कुलुई इत्यादि वर्ग अधिक प्रचलित हैं। इसमे भी यदि हम इस लिपि को समग्र भाषा की लिपि ना कहकर बोलियों की लिपि कहें तो अधिक उचित होगा। यह कहना सही होगा कि इस लिपि में बदलाव ना केवल त्रुटियों के कारण अपितु स्थानीय बोलियों के अनुसार भी हुआ है।
1896 में प्रकाशित पुस्तक ‘The Kulu Dialect of Hindi’ में टांकरी लिपि का कुलुई स्वरूप दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्रकार ऊपरी घाटी और दूसरा निचली घाटी का है। कुल्लू का एक और प्रचलित प्रकार जो मंडयाली टांकरी से साम्य रखता है वह पुस्तक में नहीं दिया गया। आंतरिक और बाह्य सराजी टांकरी मंडयाली टांकरी से मिलती है। इसमे कुल्लू और मंडी की टांकरी के अक्षरों का समावेश देखने को मिलता है। कुछ नए अक्षरान्तर इस कारण भी देखने मे आते हैं। भाषाई उच्चारण के अंतरों में एक उदाहरण यह है कि कुलुई बोली में ‘व’ का उच्चारण नहीं होता। इसके स्थान पर या तो स्पष्ट रूप से ‘ब’ का उच्चारण होता है या फिर ‘उआ’ कहा जाता है। अतः यहां ‘ब’ या ‘व’ लिखने के लिए टांकरी में समान अक्षर का भी प्रयोग प्रचलित है। टांकरी के अक्षरों का अंतर हमें डॉ. रीता शर्मा द्वारा लिखी गई टांकरी की आरंभिक पुस्तकों में से एक टांकरी पुस्तिका में दिखाई देता है। यही तालिका हमें कुल्लू से टांकरी लिपि के प्रसिद्ध विद्वान स्व. ख़ूबराम खुशदिल जी की ‘टांकरी पाठमाला में भी मिलती है। ‘मंडयाली टांकरी’ नाम से टांकरी पर पुस्तक प्रकाशित कर चुके ‘जगदीश कपूर’ जी ने भी ऐसी ही तालिका अपनी पुस्तक में प्रस्तुत की है। कुछ स्थानों पर स्वरों-अक्षरों में अन्य अंतर भी दिखते हैं, जो तालिका में या पुस्तकों में सूचीबद्ध नहीं किये गए हैं। जैसे सराज घाटी के स्थान बळागाड़ के मार्कण्डेय ऋषि के मंदिर की पोथी, जिसमे देवता और मंदिर के कार्यों का हिसाब-किताब रखा जाता है, उसमें ‘अ’ की बनावट इन सभी तालिकाओं से अलग है। इस प्रकार के अंतर विभिन्न स्थानों के अभिलेखों में दिखाई देना लिपि और इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए आम बात है। उसका मूल कारण भी उपरोक्त है, लेखक द्वारा लेखन शैली के लिए अपनाए जाने वाले अपने अलग तरीके और लेखन की त्रुटियां।
● वर्तमान समय मे टांकरी पर महत्वपूर्ण कार्य ●
टांकरी लिपि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रचलन से बाहर होने के बाद से ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। ऐसा होने से कश्मीर की शारदा लिपि समान ही इसे जानने-समझने वाले विद्वानों की संख्या समय के साथ सीमित रह गई। परंतु सरकारी विभागों और कुछ विद्वानों के प्रयासों से यह लिपि किसी कोने में जीवित रहने में सफ़ल हुई है। इस लिपि को जीवंत रखने में सबसे पहला नाम जो आता है वह है कुल्लू के कराड़सू गांव के रहने वाले स्व. ख़ूबराम खुशदिल जी का। ख़ूबराम जी टांकरी के जाने-माने विद्वान रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन काल मे ना केवल इस लिपि की अलख जगाए रखी, अपितु इस लिपि की पांडुलिपियों का पूरे प्रदेश के विभिन्न स्थानों में घूम-घूम कर संग्रह भी किया। टांकरी की पांडुलिपियों का किसी निजी व्यक्ति द्वारा किया गया सम्भवतः सबसे व्यापक संग्रह उनके घर पर मौजूद है। उसके बाद कांगड़ा के रहने वाले लोककवि हरिकृष्ण मुरारी जी ने भी इस लिपि को जीवित रखने में अपना योगदान दिया। इन्होंने लिपि के विभिन्न स्वरूपों की वर्णमालाएं तैयार करके भाषा अकादमी और विभाग संग मिलकर बहुत सी कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को इस लिपि का ज्ञान दिया। विद्यामूलक विषय मे डॉक्टर किशोरी चंदेल जी इस समय टांकरी पर व्यापक शोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने कुल्लू घाटी के देवताओं के मोहरों पर लिखी लिपि को पढ़कर अनुवाद किया और इसपर शोधपत्र भी लिखा। इस शोधपत्र के अलावा भी टांकरी पर उनका काम श्लाघ्य है। मंडी से जगदीश कपूर जी ने मंडयाली टांकरी पर पुस्तक लिखकर इसे पाठकों के लिए सहज बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इन सभी विद्वानों के अथक प्रयासों के अलावा ऐसे अन्य भी विद्वान रहे हैं जो टांकरी लिपि के निष्णात अनुवादक हैं। लक्ष्मण ठाकुर जी और तोबदन जी का नाम इनमें सर्वप्रथम लेना आवश्यक है। लिपि की बारीकियों और उसकी बनावट पर वैज्ञानिक अध्ययन में लक्ष्मण ठाकुर जी जहां श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं वहीं तोबदन जी इस लिपि के सर्वश्रेष्ठ अनुवादकों में से एक हैं।
विभागीय स्तर पर भाषा अकादमी शिमला और ज़िला स्तरीय भाषा विभागों द्वारा दिये गए सहयोग एवं प्रोत्साहन से समय-समय पर लिपि को जीवंत बनाए रखने के लिए लगाई जाने वाली ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्यशालाएं भी समय-समय पर इसे जीवनदान देने में अपना योगदान देती रही हैं।
कांगड़ा की संस्था साम्भ द्वारा टांकरी लिपि पर 2016 में सर्वप्रथम डिजिटल फॉन्ट बनाकर उसे निशुल्क लोगों में वितरित करने से इस लिपि का सोशल मीडिया में व्यापक प्रचार हुआ है। भाषा अकादमी और भाषा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं में कुल 2000 से अधिक लोगों को टांकरी लिपि का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
सभी के अथक प्रयासों से आज यह लिपि अपनी विलुप्तप्राय स्थिति से बाहर निकलकर बहुत लोगों तक पहुंच बना पाई है और अब पहले से अधिक लोग इसको पढ़ने-समझने में सक्षम हुए हैं।
उपसंहार
टांकरी कहिए या टाकरी, पहाड़ों की इस प्रसिद्ध लिपि के अस्तित्व पर हम आंखें मूंदे नहीं रह सकते। यह केवल लिखने का एक तरीका भर नही, अपितु पहाड़ों के इतिहास का एक पूरा कालखण्ड अपने मे समेटे हुए है। टांकरी लिपि के जानकार किसी स्थानीय बुज़ुर्ग ने एक बार कहा कि कि यह ‘लाटी लिपि’ अर्थात लंगड़ी लिपि है। इसकी अपनी एक विशेषता है। बोलियों को यह आसानी से सहेज लेती है, परंतु संस्कृत जैसी वृहद व्याकरण युक्त भाषाओं का इसमे समावेश करना कठिन हो जाता है। अतः इसे बोलियों की, लोक की लिपि कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। लिपि सीखने में वैसे तो 7 से 10 दिन का ही समय लगता है, परंतु वर्णान्तर होने के कारण इसे समझने में बहुत अधिक समय लगता है। टांकरी पर उपलब्ध दस्तावेज़ों का संग्रह करने की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। टांकरी के अधिकतर दस्तावेज़ देवी-देवताओं से जुड़े होने के कारण लोगों के मन मे भ्रम रहता है कि यह कोई चमत्कारिक मंत्र या कुछ विशेष बात देवता से सम्बंधित है अतः इसे पढ़ना या इसका अनुवाद निषेध है। देवताओं के जितने मोहरों का आजतक मेरे द्वारा अनुवाद किया गया, वहां के लोग आरम्भ में सशंकित थे कि इस मोहरे में सतयुग की कोई विशेष बात लिखी होगी, या कोई मंत्र लिखा हुआ होगा। जबकि सत्यता यह है कि लगभग सभी देव-मोहरों में उस मोहरे को बनाने का समय, बनाने वाले कारीगर का नाम, विशेष दानकर्ता जैसे राजा इत्यादि यदि कोई हो तो उसका नाम, कारदार का नाम, गुर का नाम और एक-दो अन्य नामों, स्थानों के अलावा कुछ नहीं होता। परंतु इस विषय पर आम जनमानस की अज्ञानता के कारण भी अधिकतर पांडुलिपियां, जो किसी देवता के संग्रह में या किसी निजी संग्रह में हैं, अनुवाद से वंचित रह जाती हैं और पहाड़ी इतिहास का वह पक्ष धुंधला ही रह जाता है।
निःसंदेह, यह भी सत्य है कि इस लिपि का प्रयोग स्थानीय देवताओं के मंत्र-यंत्र लिखने में होता था। इसी कारण सम्भवतः लोगों के मन मे इसके अनुवाद के प्रति भय एवं सन्देह उत्पत्ति का कारण प्रतीत होता है।
यथा: स्व. पुरोहित चंद्र शेखर बेबस जी के घर से मिली टांकरी की एक पांडुलिपि में एक यंत्र बना हुआ था जिसमे एक ओर टांकरी में और दूसरी ओर नागरी में स्थानीय देवताओं का शाबर मंत्र लिखा हुआ था। जिस प्रकार वैदिक मंत्रों और शाबर मंत्रों का अंतर है उसी प्रकार हम टांकरी और शारदा, नागरी का अंतर मान सकते हैं। इस कारण और दूसरी ओर लिपि का ज्ञान ना होने से और स्थानीय विद्याओं की टांकरी में लिखी पुस्तकों का सहजता से बाहर ना आ पाने से ना केवल लिपि के संरक्षण, संवर्धन का कार्य रुकता है अपितु यह स्थिति सम्बंधित विद्याओं के लोप का कारण भी बन जाती है। टांकरी लिपि के संरक्षण के साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में प्रचलित रही सभी लिपियों का संरक्षण आवश्यक है। पाबूची, पण्डवानी, चण्डवाणी, भट्टाक्षरी इत्यादि लिपियों पर भी काम होना आवश्यक है। टांकरी को डिजिटल फॉन्ट के रूप में विकसित करने के बाद अन्य लिपियों के फॉन्ट बनाने की आवश्यकता है। ताकि इन्हें लंबे समय के लिए सुरक्षित किया जा सके। यह सत्य है कि इंटरनेट के माध्यम से आज टांकरी लिपि को प्रचार-प्रसार का साधन मिल चुका है। परंतु हमारा सामूहिक प्रयास ही हमारी इस लिपि को जीवंत बनाए रखेगा, यह हमें समय रहते समझना चाहिए। ताकि हमारी पहाड़ों की लिपि जीवित रहे और हमारे पहाड़ों का इतिहास उस लिपि में जीवंत रहे।
––––––––––––––––––
यतिन पंडित , कुल्लू
––––––––––––––––––